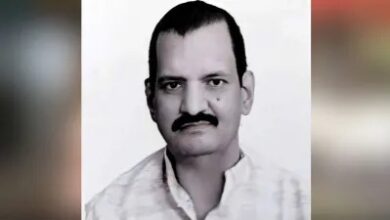महामारी और भू-राजनीतिक तनाव ने खोलीं वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की कमजोरियां
कोविड-19 महामारी और लगातार बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की गंभीर कमजोरियों को उजागर कर दिया है। इससे डिफेंस इंडस्ट्री में देरी, लागत वृद्धि और संचालन बाधाएं पैदा हुईं। ऐसे समय में जब समयबद्धता बेहद अहम है, लचीलापन और अनुकूलता रक्षा निर्माताओं की रणनीतिक जरूरत बन चुकी है। कंपनियां एजाइल सप्लाई चेन, डिजिटल परिवर्तन, वर्कफोर्स आधुनिकीकरण और उन्नत अनुसंधान एवं विकास (R&D) को अपनाकर इन चुनौतियों का समाधान कर रही हैं।
“जस्ट-इन-टाइम” से “जस्ट-इन-केस” मॉडल की ओर रुख
पारंपरिक रूप से रक्षा कंपनियां वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर थीं, जो जस्ट-इन-टाइम मॉडल पर काम करती थीं। लेकिन हाल की वैश्विक घटनाओं और व्यापार प्रतिबंधों ने इस मॉडल की कमजोरियों को उजागर किया। अब उद्योग “जस्ट-इन-केस” मॉडल की ओर बढ़ रहा है, जिसमें वैकल्पिक योजनाएं (Plan B और Plan C) तैयार रहती हैं ताकि संचालन में बाधा न आए। इस मॉडल में आपूर्ति विविधता, स्टॉक बफर, और महत्वपूर्ण घटकों का निकट-स्थानीयकरण अहम हैं।
‘मेक इन इंडिया’ से मिली घरेलू रक्षा निर्माण को मजबूती
भारत की मेक इन इंडिया पहल ने घरेलू रक्षा उत्पादन को और अधिक लचीला व सशक्त बनाया है। आयात पर निर्भरता घटाकर और स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देकर यह पहल न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ कर रही है, बल्कि वैश्विक आपूर्ति झटकों से कंपनियों को बचा भी रही है। कई भारतीय कंपनियां अब केवल अंतिम असेंबली ही नहीं, बल्कि उप-प्रणालियों और घटकों का भी स्थानीयकरण कर रही हैं, जिससे रणनीतिक आत्मनिर्भरता बढ़ रही है।
डिजिटल परिवर्तन: भविष्य की मजबूती की नींव
डिजिटलीकरण रक्षा निर्माण में लचीलापन बढ़ाने का प्रमुख आधार बन रहा है। डिजिटल ट्विन, AI आधारित प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, और रीयल-टाइम एनालिटिक्स जैसी तकनीकों से कंपनियां संभावित बाधाओं का पूर्वानुमान लगा पा रही हैं और उत्पादन को बेहतर बना रही हैं। वर्चुअल सिमुलेशन के जरिए वे विभिन्न संकटों (जैसे सामग्री की कमी या साइबर अटैक) के लिए अपनी तैयारियों का मूल्यांकन कर सकती हैं।
साइबर सुरक्षा: संचालन स्थिरता की रीढ़
डिजिटल सिस्टम पर बढ़ती निर्भरता के साथ साइबर सुरक्षा रक्षा निर्माताओं के लिए प्राथमिक चिंता बन गई है। अब यह सिर्फ आईटी का नहीं, बल्कि एक बिजनेस-क्रिटिकल फंक्शन है। कंपनियां अब लेयर-आधारित सुरक्षा फ्रेमवर्क, एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, और फायरवॉल में निवेश कर रही हैं। AI और ML के ज़रिए नए खतरों को स्वतः पहचान कर निष्क्रिय किया जा रहा है।
कुशल कार्यबल: तकनीक के साथ तालमेल
सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि कर्मचारियों को भी नई तकनीकों के अनुरूप ढालना जरूरी है। कंपनियां डिजिटल स्किल्स, सिस्टम थिंकिंग, और साइबर अवेयरनेस पर आधारित रि-स्किलिंग प्रोग्राम्स चला रही हैं। क्रॉस-फंक्शनल स्किल्स विकसित करने से कर्मचारियों की लचीलता बढ़ रही है। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों, आईटीआई और स्किलिंग सेंटर्स से मिलकर प्रशिक्षित टैलेंट तैयार किया जा रहा है।
सार्वजनिक-निजी भागीदारी: नवाचार और स्थिरता की दिशा में
रक्षा उद्योग में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह साझेदारियां संयुक्त नवाचार, जोखिम साझेदारी, और सरकारी समर्थन के ज़रिए स्थायित्व सुनिश्चित कर रही हैं। इससे कंपनियों को उन्नत तकनीकों तक पहुंच, दीर्घकालिक ऑर्डर्स और संकट के समय भी निरंतरता मिलती है।
वैश्विक रक्षा हब बनने की दिशा में भारत
आज के अनिश्चित वैश्विक माहौल में, लचीलापन एक रणनीतिक प्राथमिकता बन चुका है। भारतीय रक्षा निर्माता सुरक्षित, अनुकूलनीय, और तेज़ प्रतिक्रिया वाली प्रणालियां विकसित कर रहे हैं। नीति समर्थन (जैसे मेक इन इंडिया) और नवाचार के सही मिश्रण के साथ, भारत अब एक प्रतिक्रियात्मक आपूर्तिकर्ता से वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है।